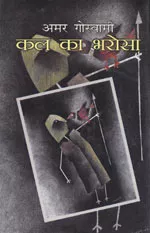|
कहानी संग्रह >> कल का भरोसा कल का भरोसाअमर गोस्वामी
|
270 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है श्रेष्ठ कहानी संग्रह...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
जहाँ आजादी के बाद पाँच दशक आम आदमी के विपन्न और अनवरत असहाय होने का काल रहा है वहीं समकालीन साहित्य में इस दुर्भाग्यपूर्ण सच का सामना प्रायः सैद्धांतिक लबादा ओढ़कर परिवर्तन के मोहर नारों के दोहराव के साथ ही किया जाता रहा है। एक लंबे दौर से कहानियों में आम आदमी के विजय-ध्वज को चटख रंगों से रँगे जाने के साथ-साथ काल्पनिक मुक्ति का वज्र निर्घोष भी सुनाई देता रहा है।
अपनी बात
आज से तीस-पैंतीस साल पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि मैं क्यों लिखता हूँ,
तो उस वक्त जो जवाब होता, वह आज मैं नहीं दे सकता। वह युवा वय के अति
उत्साह का भावुकता भरा दौर था। लगता-चीजें मेरी मुट्ठी में हैं और लेखन
में मेरी सक्रियता से बहुत कुछ बदल जाएगा। तथाकथित प्रगतिशील मित्रों की
चपलताओं से भी कुछ ऐसी धारणा बन गई थी।
मुझमें आज न वैसे उत्साह का अतिरेक है, न भावुकता का आंदोलन ही है। समाज और जीवन का यथार्थ बहुत कुछ समझ में आ गया है। हिंदी पट्टी में पढ़े-लिखों की साहित्य के प्रति छाई उदासीनता और सारे समय पैसे व मनोरंजन के पीछे भागने की मानसिकता ने भी निरंतर क्षुब्ध ही किया है। जो पढ़ना ही नहीं चाहते, लेखक उन्हें साहित्य पढ़ने के लिए विवश कैसे करे ? उसपर लेखकों को पूछता ही कौन है-न अखबारवाले न मीडियावाले और न सत्तातंत्र के विभिन्न आसंदियों पर विराजमान जनसंपर्क से जुड़े लोग ही। लेखक की हैसियत को आँकना इन सभी के बूते के बाहर है। जो एक अच्छी पुस्तक पर अपनी राय नहीं दे सकते, उस लेखक के बारे में कुछ बता नहीं सकते, वे लेखकों को हेय तो समझेंगे ही। जीवन में बहुत कुछ प्रचार पर चलता है। बिना प्रचार के हिंदी साहित्य सही पाठकों तक न पहुँच पाने के कारण गोदामों में या सेल्फों-अलमारियों में सजाने की वस्तु हो गया है। इन सबसे बचने के लिए कुछ गुटीय लेखकों ने जरूर अपने प्रचार का एक सिलसिला बना रखा है। इससे वे व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित हो जाते हैं; पर हिन्दी साहित्य तथा अन्य साहित्कारों का इससे कोई भला नहीं होता। यह तो भला हो हिन्दी प्रकाशकों का। जो व्यवसाय के कारण लेखकों की पुस्तकें छापते रहते हैं, जिससे लेखकों को आर्थिक रूप से भले ही कोई खास लाभ न मिलता हो, पर कुछ पुस्तकें पढ़नेवाली जनता तक पहुँच तो जाती हैं।
कमोबेश यह अपने हिंदी समाज की स्थिति है, एक रेगिस्तान जैसी स्थिति, जहाँ कभी-कभार कोई नखलिस्तान दिख जाता है। ऐसे माहौल में रहकर भी मैं क्यों लिखता हूँ? ऐसी क्या विवशता है मेरे साथ ? ऐसी हालत में, जबकि न जाने कितने लोग अपने यौवनजन्य उत्साह के समाप्त होने और किन्ही कारणों से लिखना बंद कर चुके हैं। मेरा लिखना क्या ‘स्वांतः सुखाय’ है या मन की मौज है, जो मुझसे लिखवाती रहती है, जैसा कि हाशिए पर बैठे बहुत से लोग अपने बारे में कहते रहते हैं।
मैं नहीं जानता कि कहानीकार के तौर पर मेरी स्थित क्या है ? इसमें बड़ा ‘कन्फ्यूजन’ है। मगर इतना मैं बतौर लेखक बता देना चाहता हूँ कि मैं ‘स्वांतः सुखाय’ नहीं लिखता, ‘पर सुखाय’ लिखता हूँ। यह ‘पर सुखाय’ ही मेरा ‘स्वांतः सुखाय है। मनुष्य के प्रति मेरी चिन्ताएँ मुझे लिखने के लिए उकसाती हैं। दरअसल और कुछ करने के लिए मेरी क्षमता बहुत सीमित है और स्वभाव भी अंतर्मुखी है, थोड़ा कायर भी हूँ। तो ऐसा आदमी क्या चुपचाप बैठ जाए और कोई प्रतिरोध न करे ? अपनी असहायता ने मुझमें प्रतिरोध को जन्म दिया है। मैं जीवन में अन्याय के प्रतिरोध में अपनी कलम को मुखर बनाने की चेष्टा करता रहता हूँ। किसी सर्वहारा के पक्ष में कलम बोलती है तो मुझे सुकून मिलता है और यह सुकून मुझे उन सभी लेखकों की कलम से मिलता है जो बोलती हैं-वे भले ही कोई पंथानुगामी हों। लिखना इसलिए मेरे लिए जरूरी हो गया है और यह एक नशे की आदत में बदल गया है। आप लिखें और लगे की आपकी कलम से देश का लोकतन्त्र बोल रहा है, इससे सुखद अहसास और क्या हो सकता है ! लेखन ने लगातार मुझे दायित्वशील बनने के लिए बाध्य किया है, इसलिए औरों की अपने प्रति निंदा, प्रशंसा या उपेक्षा का मेरे लिए अर्थ नहीं रह गया है।
कई विधाओं में लिखने के बावजूद मैं खुद को कथाकार ही मानता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी कहानियों में पाठकों को वे चुनौतियाँ तथा असहमतियाँ नजर आएँ, जिनमें आम भारतीय जूझता रहता है और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए खून-पसीना एक करता रहता है। उसकी सामयिक पराजय में भी मुझे महिमा नजर आती है तथा कमजोर का बल, जो आनेवाले कल के प्रति भरोसा जगाता है।
मुझमें आज न वैसे उत्साह का अतिरेक है, न भावुकता का आंदोलन ही है। समाज और जीवन का यथार्थ बहुत कुछ समझ में आ गया है। हिंदी पट्टी में पढ़े-लिखों की साहित्य के प्रति छाई उदासीनता और सारे समय पैसे व मनोरंजन के पीछे भागने की मानसिकता ने भी निरंतर क्षुब्ध ही किया है। जो पढ़ना ही नहीं चाहते, लेखक उन्हें साहित्य पढ़ने के लिए विवश कैसे करे ? उसपर लेखकों को पूछता ही कौन है-न अखबारवाले न मीडियावाले और न सत्तातंत्र के विभिन्न आसंदियों पर विराजमान जनसंपर्क से जुड़े लोग ही। लेखक की हैसियत को आँकना इन सभी के बूते के बाहर है। जो एक अच्छी पुस्तक पर अपनी राय नहीं दे सकते, उस लेखक के बारे में कुछ बता नहीं सकते, वे लेखकों को हेय तो समझेंगे ही। जीवन में बहुत कुछ प्रचार पर चलता है। बिना प्रचार के हिंदी साहित्य सही पाठकों तक न पहुँच पाने के कारण गोदामों में या सेल्फों-अलमारियों में सजाने की वस्तु हो गया है। इन सबसे बचने के लिए कुछ गुटीय लेखकों ने जरूर अपने प्रचार का एक सिलसिला बना रखा है। इससे वे व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित हो जाते हैं; पर हिन्दी साहित्य तथा अन्य साहित्कारों का इससे कोई भला नहीं होता। यह तो भला हो हिन्दी प्रकाशकों का। जो व्यवसाय के कारण लेखकों की पुस्तकें छापते रहते हैं, जिससे लेखकों को आर्थिक रूप से भले ही कोई खास लाभ न मिलता हो, पर कुछ पुस्तकें पढ़नेवाली जनता तक पहुँच तो जाती हैं।
कमोबेश यह अपने हिंदी समाज की स्थिति है, एक रेगिस्तान जैसी स्थिति, जहाँ कभी-कभार कोई नखलिस्तान दिख जाता है। ऐसे माहौल में रहकर भी मैं क्यों लिखता हूँ? ऐसी क्या विवशता है मेरे साथ ? ऐसी हालत में, जबकि न जाने कितने लोग अपने यौवनजन्य उत्साह के समाप्त होने और किन्ही कारणों से लिखना बंद कर चुके हैं। मेरा लिखना क्या ‘स्वांतः सुखाय’ है या मन की मौज है, जो मुझसे लिखवाती रहती है, जैसा कि हाशिए पर बैठे बहुत से लोग अपने बारे में कहते रहते हैं।
मैं नहीं जानता कि कहानीकार के तौर पर मेरी स्थित क्या है ? इसमें बड़ा ‘कन्फ्यूजन’ है। मगर इतना मैं बतौर लेखक बता देना चाहता हूँ कि मैं ‘स्वांतः सुखाय’ नहीं लिखता, ‘पर सुखाय’ लिखता हूँ। यह ‘पर सुखाय’ ही मेरा ‘स्वांतः सुखाय है। मनुष्य के प्रति मेरी चिन्ताएँ मुझे लिखने के लिए उकसाती हैं। दरअसल और कुछ करने के लिए मेरी क्षमता बहुत सीमित है और स्वभाव भी अंतर्मुखी है, थोड़ा कायर भी हूँ। तो ऐसा आदमी क्या चुपचाप बैठ जाए और कोई प्रतिरोध न करे ? अपनी असहायता ने मुझमें प्रतिरोध को जन्म दिया है। मैं जीवन में अन्याय के प्रतिरोध में अपनी कलम को मुखर बनाने की चेष्टा करता रहता हूँ। किसी सर्वहारा के पक्ष में कलम बोलती है तो मुझे सुकून मिलता है और यह सुकून मुझे उन सभी लेखकों की कलम से मिलता है जो बोलती हैं-वे भले ही कोई पंथानुगामी हों। लिखना इसलिए मेरे लिए जरूरी हो गया है और यह एक नशे की आदत में बदल गया है। आप लिखें और लगे की आपकी कलम से देश का लोकतन्त्र बोल रहा है, इससे सुखद अहसास और क्या हो सकता है ! लेखन ने लगातार मुझे दायित्वशील बनने के लिए बाध्य किया है, इसलिए औरों की अपने प्रति निंदा, प्रशंसा या उपेक्षा का मेरे लिए अर्थ नहीं रह गया है।
कई विधाओं में लिखने के बावजूद मैं खुद को कथाकार ही मानता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी कहानियों में पाठकों को वे चुनौतियाँ तथा असहमतियाँ नजर आएँ, जिनमें आम भारतीय जूझता रहता है और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए खून-पसीना एक करता रहता है। उसकी सामयिक पराजय में भी मुझे महिमा नजर आती है तथा कमजोर का बल, जो आनेवाले कल के प्रति भरोसा जगाता है।
फाँस
बाहर धूप का दमामा बज रहा था। हवा सिकुड़कर बासी फूल बन गई थी। जो बाहर
थे, वे गन्दे पानी से नहाए लग रहे थे। कार के अन्दर की कृत्रिम ठंड में
मलिक साहब अपने एक खास सपने की फाइल खोल उसमें दस्तखत कर रहे थे। तभी उनकी
कार चलते-चलते अचानक रूक गई। मलिक साहब का ध्यान टूट गया। दस्तखत करने की
बात वे भूल गए। उन्होंने ड्राइवर से पूछा, ‘क्या बात है अचानक
गाड़ी क्यों रोक दी ?’
ड्राइवर ने सामने इशारा करके कहा, ‘साहब उधर एक चनेवाला बैठा है।’ मलिक साहब ने देखा, दोपहर के सन्नाटे में एक पेड़ के नीचे वह चने वाला बैठा था- अपनी टोकरी में उबले चने सजाए। उन्हीं काले चनों से वह अपनी खुशियाँ साकार करना चाहता था। चनेवाले के आप-पास एक खालीपन था जिसे थोड़ी दूर बैठा एक सताया हुआ कुत्ता भर रहा था।
मलिक साहब ने अपने ड्राइवर की आँखों में देखा, उसके भावों को ताड़ने की कोशिश की, पर उसकी आँखों में कुछ भी नहीं था, वे खाली जेब जैसी लगीं। वे ड्राइवर से बोले, ‘जाओ, चने ले आओ। उस वक्त उनकी आवाज में जमीन नहीं थी। बस धूल थी। उन्होंने पाँच का एक चमचमाता सिक्का आगे बढ़ा दिया। ड्राइवर गाड़ी का गेट खोल कर उतर गया। उसे पास आते हुए देखकर जड़ चने वाला चैतन्य हो गया। कुछ दूर बैठे कुत्ते पर भी प्रतिक्रिया हुई। उसने कान खड़े करके दुम हिलाई। उससे कुछ मक्खियाँ विरक्त हुईं और आस-पास की हवा की भृकुटि टेढ़ी हुई। चनेवाले ने एक कटे हुए छोटे रूमालनुमा काग़ज पर थोड़े चने निकाले। उसमें नीबू के रस की कुछ बूँदे डालकर मसाला बुरका, मूली प्याज की कतरने डालीं, बच्चे की तरह हिलाया-डुलाया, फिर उसे एक दूसरे रूमालनुमा कागज में डालकर सिक्के विनिमय में ड्राइवर को थमा दिया। ड्राइवर ने उसे किसी बीमार औरत की तरह सँभाला। लौटकर उसने उसी तरह मलिक साहब की ओर बढ़ा दिया।
मलिक साहब उसे देखते ही चिहुँके। फिर बोले, ‘इसे तुम खा लो। इस वक्त मेरा मन नहीं है।’
ड्राइवर मन-ही-मन मुसकराया। उसे पता था, मलिक साहब ऐसा ही करते थे। कहीं भी किसी चने वाले को खाली बैठे देखते तो उससे चने खरीद लेते, पर खाने के नाम पर हमेशा कन्नी काट जाते। उसे अपने ड्राइवर को खिला देते थे। ड्राइवर उनकी इस आदत से हैरान होता, मन-ही-मन हँसता भी। खैर, उसको क्या ! मुफ्त में उसे चने खाने को मिल जाते। वह अपना स्वास्थ्य बना रहा था।
मलिक साहब की इस आदत के बारे में धीरे-धीरे सभी को पता चल गया था। गुप्त बात की तरह यह सार्वजनिक हो गई थी। लोग इसे उसकी सनक समझने लगे थे। कुछ की धारणा पक्की हो गई थी कि पिछले जन्म में मलिक साहब जरूर घोड़ा रहे होंगे, नहीं तो ‘जहाँ चना वहीं घोड़ा’ वाली यह हरकत वे क्यों करते ?
मलिक साहब की पत्नी भी उनकी इस आदत से परेशान थी। मलिक साहब कब क्या कर बैठें, कुछ कहना मुश्किल था एक बार उन्हें आधी रात को हलवा खाने का मन हुआ तो बिस्तर से उठकर न सिर्फ खुद हलवा बनाया, बल्कि सबको जगाकर खिलाया भी। हलवा जैसा भी बना हो, सबको उसकी भरपूर प्रशंसा करनी पड़ी। उसी तरह एक बार उन्हें करेला खाने की धुन सवार हुई। वे महीने भर तक सुबह-शाम करेले की तरह-तरह की सब्जियाँ खाते रहे। उस मानसिकता में एक दिन बहुत खुश होकर उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक कविता लिखी-
ड्राइवर ने सामने इशारा करके कहा, ‘साहब उधर एक चनेवाला बैठा है।’ मलिक साहब ने देखा, दोपहर के सन्नाटे में एक पेड़ के नीचे वह चने वाला बैठा था- अपनी टोकरी में उबले चने सजाए। उन्हीं काले चनों से वह अपनी खुशियाँ साकार करना चाहता था। चनेवाले के आप-पास एक खालीपन था जिसे थोड़ी दूर बैठा एक सताया हुआ कुत्ता भर रहा था।
मलिक साहब ने अपने ड्राइवर की आँखों में देखा, उसके भावों को ताड़ने की कोशिश की, पर उसकी आँखों में कुछ भी नहीं था, वे खाली जेब जैसी लगीं। वे ड्राइवर से बोले, ‘जाओ, चने ले आओ। उस वक्त उनकी आवाज में जमीन नहीं थी। बस धूल थी। उन्होंने पाँच का एक चमचमाता सिक्का आगे बढ़ा दिया। ड्राइवर गाड़ी का गेट खोल कर उतर गया। उसे पास आते हुए देखकर जड़ चने वाला चैतन्य हो गया। कुछ दूर बैठे कुत्ते पर भी प्रतिक्रिया हुई। उसने कान खड़े करके दुम हिलाई। उससे कुछ मक्खियाँ विरक्त हुईं और आस-पास की हवा की भृकुटि टेढ़ी हुई। चनेवाले ने एक कटे हुए छोटे रूमालनुमा काग़ज पर थोड़े चने निकाले। उसमें नीबू के रस की कुछ बूँदे डालकर मसाला बुरका, मूली प्याज की कतरने डालीं, बच्चे की तरह हिलाया-डुलाया, फिर उसे एक दूसरे रूमालनुमा कागज में डालकर सिक्के विनिमय में ड्राइवर को थमा दिया। ड्राइवर ने उसे किसी बीमार औरत की तरह सँभाला। लौटकर उसने उसी तरह मलिक साहब की ओर बढ़ा दिया।
मलिक साहब उसे देखते ही चिहुँके। फिर बोले, ‘इसे तुम खा लो। इस वक्त मेरा मन नहीं है।’
ड्राइवर मन-ही-मन मुसकराया। उसे पता था, मलिक साहब ऐसा ही करते थे। कहीं भी किसी चने वाले को खाली बैठे देखते तो उससे चने खरीद लेते, पर खाने के नाम पर हमेशा कन्नी काट जाते। उसे अपने ड्राइवर को खिला देते थे। ड्राइवर उनकी इस आदत से हैरान होता, मन-ही-मन हँसता भी। खैर, उसको क्या ! मुफ्त में उसे चने खाने को मिल जाते। वह अपना स्वास्थ्य बना रहा था।
मलिक साहब की इस आदत के बारे में धीरे-धीरे सभी को पता चल गया था। गुप्त बात की तरह यह सार्वजनिक हो गई थी। लोग इसे उसकी सनक समझने लगे थे। कुछ की धारणा पक्की हो गई थी कि पिछले जन्म में मलिक साहब जरूर घोड़ा रहे होंगे, नहीं तो ‘जहाँ चना वहीं घोड़ा’ वाली यह हरकत वे क्यों करते ?
मलिक साहब की पत्नी भी उनकी इस आदत से परेशान थी। मलिक साहब कब क्या कर बैठें, कुछ कहना मुश्किल था एक बार उन्हें आधी रात को हलवा खाने का मन हुआ तो बिस्तर से उठकर न सिर्फ खुद हलवा बनाया, बल्कि सबको जगाकर खिलाया भी। हलवा जैसा भी बना हो, सबको उसकी भरपूर प्रशंसा करनी पड़ी। उसी तरह एक बार उन्हें करेला खाने की धुन सवार हुई। वे महीने भर तक सुबह-शाम करेले की तरह-तरह की सब्जियाँ खाते रहे। उस मानसिकता में एक दिन बहुत खुश होकर उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक कविता लिखी-
‘मेरी प्राणप्यारी !
मेरे जीवन की थाली में
तुम हो करेले की तरकारी !
मेरे जीवन की थाली में
तुम हो करेले की तरकारी !
कविता कुछ लम्बी थी। मगर इतना सुनते ही मिसेज मलिक ने जो कोलाहल किया,
उससे मलिक साहब के हाथों के तोते उड़ गए और शान्ति भंग होने के डर से उनकी
बोलती बंद हो गई। कविता में भी पूरी और करेले की सब्जी थी। पत्नी ने घर
में करेले पर कर्फ्यू लगा दिया। मगर कर्फ्यू करेले पर था चने पर तो था
नहीं, इसलिए एक दिन अपनी धुन में मलिक साहब बाहर से घर में आए तो उनके हाथ
में मसालेदार उबले चनों का डोगा था। उन्होंने उसे पत्नी को थमाकर कहा,
‘लो खाओ।’
मिसेज मलिक उस परिवार से आई थीं, जहाँ सबकुछ डिब्बा बंद आता था। बाहर की खुली चीजें वे कभी खाती नहीं थी। काले चनों को देखकर वे भड़क गईं। बोलीं, ‘तुमने मुझे जानवर समझा है ? क्या ले आए मेरे लिए ? मैं कोई काम वाली बाई हूँ, जो सबकुछ खा लूँगी ? यही तुम्हारी पंसद है ? मुझे तो शर्म आती है।’
‘सॉरी मगर देश की बहुत बड़ी आबादी इसे पसन्द करती है। सोचा तुम्हें भी पंसद होंगे। औरतों को ऐसी चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं।
‘मैं वैसी औरत नहीं हूँ।’
तो दूसरी औरत हो ?’
‘नहीं तुम्हारी औरत हूँ , मिसेज मलिक ! मैं फुटपाथ की गंदी चीजें नहीं खाती। बाइ द वे, तुम्हें चने कब से पसंद आने लगे ? एक बार जब मैंने चने की सब्जी बनाई थी तो तुमने कितना नाक-भौं सिकोड़ा था !’
‘अब क्या बताऊँ, मन हुआ तो लेता आया। ज्यादा कुछ सोचा नहीं।’
‘लोग यों ही तुम्हें सनकी नहीं कहते। चलूँ, इन्हें डस्टबिन में फेंक आऊँ। तुमने मेरा काम बढ़ा दिया।’
किसी गरीब को दे देना। आखिर अन्न है। अपनी बाई को दे दो।’
‘उसकी तबियत खराब हो जाएगी तो भुगतना हमें ही पड़ेगा।’
‘जैसा तुम ठीक समझो।’ मलिक साहब ने हथियार डाल दिए।
चनों के प्रति मलिक साहब का कभी प्रेम नहीं था, यह सच है। वे अपने हाथ से भी कभी कोई चीज नहीं खरीदते थे। ठेलों और फुटपाथ की चीजों से उन्हें कभी कोई लगाव नहीं रहा। अब उनकी जिन्दगी में फुटपाथ था ही नहीं। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए फुटपाथ से चने खरीदकर किसी और को खिला देना हैरत की बात थी। पर इस बारे में मलिक साहब जैसे बड़े अफसर से किसी को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। बस, पीठ पीछे लोग तरह-तरह की अटकलें लगाते-अखवारवालों की तरह।
उनके प्रति सहानुभूति जताते हुए कोई कहता, ‘अरे भाई, चने ही तो खरीदते हैं, कुछ गलत काम तो नहीं करते। और लोग तो न जाने क्या-क्या करते हैं। और लोग तो जाने क्या-क्या खरीदते हैं।
‘खरीदते हैं तो खुद खाते क्यों नहीं ?’ कोई कहता।
‘यह कैसे कह सकते हो ?
‘ड्राइवर खुद कहता है।
‘हो सकता है, दूसरों को खिलाना अच्छा लगता हो, खासतौर से ड्राइवर को। यह तो अच्छी बात है।’
‘खिलाना ही हो तो फल वगैरह खिलाएँ, लड्डू-कलाकन्द खिलाएँ हलवा कचौड़ी खिलाएँ। हमें भी खिलाएँ। पर ऐसा मामूली चना !’
‘हो सकता है, कोई मनौती माँगी हो या कोई व्रत किया हो, इसलिए खिलाते हों।’
‘होगा हमें क्या ! कहाँ ऐसे खूसट कंजूस की चर्चा छेड़ दी। चर्चा ही करनी है तो कुछ और करें।
‘जैसे कि भ्रष्टाचार और बलात्कार, बढ़ती कीमतें और बाजार, बीवियों का शौहरों पर अत्याचार। यही सब ?,
लोग हँसने लगे। किसी ने कहा, ‘हम लोग चर्चा करने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं ?’
‘करने का इतना ही मन है तो चलो, आंदोलन करें।’
‘आंदोलन कोई पेशाब नहीं है कि जब मन आया कर आए।’
‘ये जो अपने नेता लोग कुछ-न-कुछ करते रहते हैं, वो ?’
‘तो फिर पहले नेता बनो। नेता बनने के लिए पहले बदनाम बनो। पब्लिक को लूटो।’
‘ठीक है, हम भी लूटेंगे। नेता बनना है।’
‘क्या लूटोगे ? कुतुबमीनार ?’
‘वाह क्या बात कही। ऐसी ही ऊँची चीजें लूटने का मजा है।’
‘सही कहा, पर उसे लूटकर रखेंगे कहाँ ? छिपाना मुश्किल है।’
‘कोई बात नहीं जब तक इतना बड़ा गड्ढा नहीं खोद लेते तब तक लूट की योजना कैंसिल।’
किसी और ने कहा, ‘रहे मूर्ख ही। योजना बनाना भी नहीं आता। उसमें भी अपना घाटा। रहे पूरे पब्लिक ही।’
किसी और ने टिप्पणी की, ‘भैये, गड्ढा पब्लिक के लिए खोदा जाता है, कुतुबमीनार के लिए नहीं ।’
लोग ठहाके लगाने लगे। किसी ने कहा, ‘वाकई हम लोग कोई ठीक-ठाक काम नहीं कर सकते।’
‘कोशिश करते रहो। एक दिन झंडा लहराएगा।’
‘भई, छोड़ो ये सब। इतना समझ लो कि सफलता चने के रास्ते भी आती है।’ लोगों को हँसी पर विराम लगाना पड़ा। मलिक साहब उधर ही आ रहे थे। सब अदब से खड़े हो गए। सन्नाटा मकड़ी के जाले-सा खिंच गया।
मलिक साहब उनकी अनदेखी करते हुए उस सन्नाटे से गुजर गए। किसी ने धीरे से कहा, ‘काश, हममें से कोई चने वाला होता तो वे हमारी ओर भी देखते।’
मलिक साहब के दिन साहबों की तरह गुजर रहे थे- व्यस्तता और दंबगई से। दस्तखत करते और मीटिंग करते, इसकी सुनते और उसको सुनाते, बिसलरी और नैपकिन का इस्तेमाल करते हुए। एक दिन जब वे दफ्तर से बाहर निकले तो देखा कि पोर्टिको में उनकी कार नहीं थी। सुबह आते समय कार में चम्मच भर खराबी आ गई थी। मलिक साहब ने ड्राइवर से उसे ठीक कराने के लिए कहा था। उसे दफ्तर से अपने लौटने का समय भी दे दिया था। संयोग से आज वे कुछ पहले ही निकल आए थे। ध्यान नहीं था नहीं तो अपने निजी सचिव से पहले पता करवा लेते। अब जब वे बाहर आ गए थे तो दुबारा अपने कमरे में जाने का उनका मन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, कुछ आप-पास का जायजा ही ले लें। इस तरह खुले में निकले बहुत दिन हो गए थे। तभी उनके एक सहयोगी अफसर ने पूछा, ‘मलिक साहब खड़े क्यों हैं ? कार कहीं गई है क्या ? कहाँ चलना है आपको ? आइए, ड्रॉप कर दूँ।’
जवाब में उन्होंने कहा, ‘थैंक्स, आप चलिए। मेरी कार अभी आती होगी।’ मलिक साहब टहलते हुए गेट के बाहर निकले। फुटपाथ पर आए। बाहर गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। लगा, स्टार्ट की सीटी बजते ही वे सब सीना ताने दौड़ पड़ेंगी। वे उधर से होते हुए उसी भवन के दूसरे फाटक के पास पहुँचे। उधर भी काफी गहमागहमी थी। जो भी था, वह बहुत अच्छा था। आस-पास के भवन तो महलों से बढ़कर थे ही, फुटपाथ भी लाजवाब था। उन्हें उस पर चलने का मन हुआ। उनका मन उस वक्त उनके बदन से काफी हलका लग रहा था, हालाँकि उनका बदन भी बुरा नहीं था। काफी तना हुआ तन था। उन्हें आस-पास सब गुब्बारे से लग रहे थे-रंग-बिरंगे, हलके-हलके। एक गुब्बारे वाले को देखकर खयाल आया कि वह कभी भी फट जाता। वैसे आतंकवादी हर किसी को गुब्बारे की तरह ही फोड़ रहे हैं। अचानक उनकी नजर एक चने वाले पर पड़ी। वह अपनी टोकरी सजाए हर आदमी में अपने ग्राहक की संभावना तलाश रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा कुछ था कि मलिक साहब कुछ देर तक उसे देखते रहे। उसे देखकर उन्हें किसी का चेहरा याद आ गया। उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश की। नहीं, यह कोई और था। उन्हें वर्षों पहले के एक दिन की याद आ गई। संयोग से वह घटना इसी जगह घटी थी। वे उस दिन भी इसी फुटपाथ से गुजर रहे थे। वे दिन कुछ और थे। उनकी हैसियत इतनी बड़ी नहीं थी। फुटपाथ की भी हैसियत आज जैसी नहीं थी। दफ्तर से बाहर निकल कर वे किसी वाहन की तलाश कर रहे थे, तभी उन्हें लगा कि कोई उन्हें बुला रहा है वह आवाज ऐसी थी कि उनके बदन में सिरहन दौड़ गई। जैसे अंधेरी रात में किसी बूढ़े पेड़ ने उन्हें पुकारा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उस आदमी को देखकर वे चौंके। उनकी भौंहों पर बल पड़े। वह एक अधेड़ चनेवाला था। उन्हें उसकी गुस्ताखी पर गुस्सा आया। फिर भी वे उसके पास चले गए। उसके बुलावे में कुछ था। पास जाकर पूछा, ‘क्या बात है ?’
चनेवाला क्षण भर उन्हें देखता रहा। वह खुद घबराया-सा था। लगा, कुछ कहते हुए वह हिचक रहा हो। उसने बड़े दबे स्वर में कहा, ‘साहब सुबह से मेरी बोहनी नहीं हुई है। बहुत गरीब आदमी हूँ। मुझसे चने खरीद लीजिए। इसे खाएँगे तो तबियत खुश हो जाएगी। सिर्फ पाँच रूपये !’
मलिक साहब की जिन्दगी में ऐसा प्रस्ताव कभी आया नहीं था। वे अकचका गए। ऐसा कुछ होगा उन्हें उम्मीद नहीं थी। उनके आस-पास काफी साफ सुथरे लोग-आ-जा रहे थे। नजदीक ही गुलदस्ते-सी नजर आनेवाली कुछ लड़कियाँ खड़ी थीं। फिर ऐसी चीजें फुटपाथ पर खरीदने से वे हमेशा बचते थे। ऐसी हालत में इस तरह से किया गया उस चनेवाले का प्रस्ताव उन्हें अनुचित लगा। उन्हें चनेवाले की हिमाकत पर गुस्सा भी आया। चनेवाले ने फिर उसी दयनीयता से कहा, खरीद लो बाबू बहुत गरीब हूँ। माँ कसम, बोहनी नहीं हुई।’
मलिक साहब ने देखा, उसकी लोहे की बालटी भरी हुई थी। एक तरफ नीबू और कुछ कटे प्याज रखे हुए थे, मसाले का एक गंदा-सा डिब्बा भी था। उबले चने मनहूस सूरत लिये पड़े हुए थे। लगा कि वे अपने सार्थक न हो पाने से खुद निराश हो गए हैं। मलिक साहब को याद नहीं पड़ा कि उन्होंने चने कब खाए थे। दरअसल चना उन्हें व्यंजनों में सर्वहारा किस्म का लगता था। वे उन्हें देखकर सहज नहीं हो पाते थे । इसलिए वे चने को करीब देखते तो मना कर देते थे। उस चनेवाले के दयनीय आग्रह का जवाब उन्होंने बहुत रूखाई से दिया। आक्रामक होकर बोले, ‘मैं चने नहीं खाता।’
‘बाबू बहुत गरीब हूँ। कुछ मदद हो जाएगी।’
मलिक साहब खीज गए। वे भुनभुनाते हुए आगे बढ़ गए। मगर चनेवाले की बातें फाँस की तरह उनके मन में गढ़ गईं। वह चेहरा गरमी के आसमान की तरह उनके साथ-साथ चलने लगा। वे कुछ परेशान हो गए गोया कोई फुंसी रगड़ खा-खा हो। एक बार सोचा, लौट जाऊँ, उससे चने न लूँ, पर पाँच रूपए दे दूँ। फिर खयाल आया, वह गरीब है तो क्या, भिखारी तो नहीं। उसका स्वाभिमान भी होगा। उन्हें किसी का सुना हुआ संवाद याद आया, ‘गरीब का अपमान ठीक नहीं।’ फिर सोचा, चने ले लूँ, किसी को दे दूँगा। पर देंगे किसे ? कोई लेगा भी क्यों ? ऐसा कोई उधर नजर भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा, ले लूँ, आगे चलकर फेंक दूँगा। पर यह भी उन्हें नहीं जँचा। फिर उन्होंने सोचा कोई परिचित मिल जाएगा तो उनके हाथ में चने देखकर क्या सोचेगा।
मलिक साहब इसी उधेड़बुन में फँसे रहे। एक अदृश्य जाला उनके चारों ओर फैल गया था। वे फैसला नहीं कर पाए और आगे बढ़ते गए। अचानक उन्हें होश आया। वे काफी दूर चले आए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वह चनेवाला नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने राहत की साँस ली, पर राहत मिली नहीं। हालत यह हुई की घर आकर वे उस चनेवाले की दयनीयता के वायरस से मुक्त नहीं हो पाए। हद तो तब हुई जब सपने में भी उसे यह कहते देखा- ‘बाबू, मैं बहुत गरीब हूँ। सुबह से बोहनी नहीं हुई। पाँच रूपये के चने खा लो।’ वे बड़बड़ाने लगे, ‘मैं चने नहीं खाता।’ मिसेज मलिक कच्ची नींद टूट जाने से नाराज होकर बोलीं, ‘आज रात में तुम्हें चने कौन खिला रहा है ? दिन में तो खाते नहीं। जाने कैसे-कैसे बेहुदे सपने देखते हो। यह लो पानी पीकर करवट लेकर सो जाओ।’ मलिक साहब ने ‘सॉरी कहा, फिर पत्नी के हाथ से पानी लिया और पीकर सो गए।
धीरे-धीरे घटना पुरानी पड़ती गई। समय बीतता रहा उन्हें अपने भीतर एक गंदा कोना नजर आने लगा, जो किसी भी रसायन से साफ नहीं हो रहा था। एक दिन कार से जाते हुए अचानक एक खाली बैठे चनेवाले पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने गाड़ी रूकवाकर उससे चने खरीद लिए और वहीं खड़े एक बच्चे को खिला दिए। धीरे-धीरे यह उनकी आदत बन गई। अब तो जब भी किसी चनेवाले को वे खाली खड़े देखते और वह उन्हें उदास नजर आता तो उससे चने जरूर खरीदते थे। दूसरे क्या सोचेंगे, इसकी चिन्ता उन्हें अब नहीं रह गई थी। उन्हें लगता कि अपना सुकून ही बड़ी बात है और वह भी तब जब वह थोड़े में मिल जाता हो। अभी तक वे अपने खयालों में खोए हुए थे। तभी उन्हें लगा कि कोई उनसे पूछ रहा है, ‘बाबू चने खिलाऊँ ? बढ़िया चने।’ मलिक साहब ने पाया की वे उस चनेवाले के ठीक सामने खड़े थे। उसके मन में कई तरह के विचार आए-गए। फिर कुछ कौतूहल हुआ। उन्होंने अपनी जेब से पाँच का सिक्का निकालकर कहा, ‘आज खिला ही दो, पर देखो इसमें कोई बीमारी न हो। साफ-साफ हों।’ चनेवाला उनकी ओर देखकर मुसकराया। बोला, ‘बाबू साहब, चिंता मत करो। खाओ तब बताना। बीस साल से यहीं पर बाबुओं की सेवा कर रहा हूँ। पहले हमारे बाप भी यहीं पर चने बेचते थे। कभी किसी ने शिकायत नहीं की।’ मलिक साहब ने चुटकी ली, ‘ खानदानी हो।’
चनेवाले ने फुरती से चने में अपना हुनर मिलाया, फिर बड़े संतोष से मलिक साहब को थमा दिया। पहली बार उन्होंने अपने लिए चने लिए थे। ले तो लिए, पर उनकी हिचकिचाहट भी बढ़ गई। खड़े-खड़े सबके सामने खाते हुए उन्हें शर्म आ रही थी। उन्होंने इधर-उधर देखा। पास ही मेंहदी की झाड़ी नजर आई। वे उसकी ओट में चले गए। चारों तरफ उन्होंने एक बार फिर से देखा, जैसे वे किसी व्यस्त चौराहे पर सड़क पार करने की विवशता में हों या किसी निषिद्ध मुहल्ले में गलत काम करने जा रहे हों। उन्होंने झट से उँगलियों से दो चने उठाकर मुँह में डाले। उसका स्वाद लेने की कोशिश की।
तभी अचानक अग्रवाल साहब आते हुए दिखे। वे सीधे उधर ही चले आ रहे थे। वे उनके पुराने साथी थे। बड़े अफसर थे। मलिक साहब ने देखा तो उनके हाथों से चने का ठोंगा छूट गया। मुँह का चना थूककर वे फुरती से आगे बढ़े। सारी चुस्ती के बावजूद उनका शरीर भीतर-ही-भीतर थरथरा रहा था।
अग्रवाल साहब का ध्यान उनकी ओर नहीं था। वे अपने में व्यस्त थे। किसी बड़े साहब की तरह इधर-उधर देखे बिना वे नाक की सीध में आगे बढ़ गए।
मिसेज मलिक उस परिवार से आई थीं, जहाँ सबकुछ डिब्बा बंद आता था। बाहर की खुली चीजें वे कभी खाती नहीं थी। काले चनों को देखकर वे भड़क गईं। बोलीं, ‘तुमने मुझे जानवर समझा है ? क्या ले आए मेरे लिए ? मैं कोई काम वाली बाई हूँ, जो सबकुछ खा लूँगी ? यही तुम्हारी पंसद है ? मुझे तो शर्म आती है।’
‘सॉरी मगर देश की बहुत बड़ी आबादी इसे पसन्द करती है। सोचा तुम्हें भी पंसद होंगे। औरतों को ऐसी चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं।
‘मैं वैसी औरत नहीं हूँ।’
तो दूसरी औरत हो ?’
‘नहीं तुम्हारी औरत हूँ , मिसेज मलिक ! मैं फुटपाथ की गंदी चीजें नहीं खाती। बाइ द वे, तुम्हें चने कब से पसंद आने लगे ? एक बार जब मैंने चने की सब्जी बनाई थी तो तुमने कितना नाक-भौं सिकोड़ा था !’
‘अब क्या बताऊँ, मन हुआ तो लेता आया। ज्यादा कुछ सोचा नहीं।’
‘लोग यों ही तुम्हें सनकी नहीं कहते। चलूँ, इन्हें डस्टबिन में फेंक आऊँ। तुमने मेरा काम बढ़ा दिया।’
किसी गरीब को दे देना। आखिर अन्न है। अपनी बाई को दे दो।’
‘उसकी तबियत खराब हो जाएगी तो भुगतना हमें ही पड़ेगा।’
‘जैसा तुम ठीक समझो।’ मलिक साहब ने हथियार डाल दिए।
चनों के प्रति मलिक साहब का कभी प्रेम नहीं था, यह सच है। वे अपने हाथ से भी कभी कोई चीज नहीं खरीदते थे। ठेलों और फुटपाथ की चीजों से उन्हें कभी कोई लगाव नहीं रहा। अब उनकी जिन्दगी में फुटपाथ था ही नहीं। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए फुटपाथ से चने खरीदकर किसी और को खिला देना हैरत की बात थी। पर इस बारे में मलिक साहब जैसे बड़े अफसर से किसी को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। बस, पीठ पीछे लोग तरह-तरह की अटकलें लगाते-अखवारवालों की तरह।
उनके प्रति सहानुभूति जताते हुए कोई कहता, ‘अरे भाई, चने ही तो खरीदते हैं, कुछ गलत काम तो नहीं करते। और लोग तो न जाने क्या-क्या करते हैं। और लोग तो जाने क्या-क्या खरीदते हैं।
‘खरीदते हैं तो खुद खाते क्यों नहीं ?’ कोई कहता।
‘यह कैसे कह सकते हो ?
‘ड्राइवर खुद कहता है।
‘हो सकता है, दूसरों को खिलाना अच्छा लगता हो, खासतौर से ड्राइवर को। यह तो अच्छी बात है।’
‘खिलाना ही हो तो फल वगैरह खिलाएँ, लड्डू-कलाकन्द खिलाएँ हलवा कचौड़ी खिलाएँ। हमें भी खिलाएँ। पर ऐसा मामूली चना !’
‘हो सकता है, कोई मनौती माँगी हो या कोई व्रत किया हो, इसलिए खिलाते हों।’
‘होगा हमें क्या ! कहाँ ऐसे खूसट कंजूस की चर्चा छेड़ दी। चर्चा ही करनी है तो कुछ और करें।
‘जैसे कि भ्रष्टाचार और बलात्कार, बढ़ती कीमतें और बाजार, बीवियों का शौहरों पर अत्याचार। यही सब ?,
लोग हँसने लगे। किसी ने कहा, ‘हम लोग चर्चा करने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं ?’
‘करने का इतना ही मन है तो चलो, आंदोलन करें।’
‘आंदोलन कोई पेशाब नहीं है कि जब मन आया कर आए।’
‘ये जो अपने नेता लोग कुछ-न-कुछ करते रहते हैं, वो ?’
‘तो फिर पहले नेता बनो। नेता बनने के लिए पहले बदनाम बनो। पब्लिक को लूटो।’
‘ठीक है, हम भी लूटेंगे। नेता बनना है।’
‘क्या लूटोगे ? कुतुबमीनार ?’
‘वाह क्या बात कही। ऐसी ही ऊँची चीजें लूटने का मजा है।’
‘सही कहा, पर उसे लूटकर रखेंगे कहाँ ? छिपाना मुश्किल है।’
‘कोई बात नहीं जब तक इतना बड़ा गड्ढा नहीं खोद लेते तब तक लूट की योजना कैंसिल।’
किसी और ने कहा, ‘रहे मूर्ख ही। योजना बनाना भी नहीं आता। उसमें भी अपना घाटा। रहे पूरे पब्लिक ही।’
किसी और ने टिप्पणी की, ‘भैये, गड्ढा पब्लिक के लिए खोदा जाता है, कुतुबमीनार के लिए नहीं ।’
लोग ठहाके लगाने लगे। किसी ने कहा, ‘वाकई हम लोग कोई ठीक-ठाक काम नहीं कर सकते।’
‘कोशिश करते रहो। एक दिन झंडा लहराएगा।’
‘भई, छोड़ो ये सब। इतना समझ लो कि सफलता चने के रास्ते भी आती है।’ लोगों को हँसी पर विराम लगाना पड़ा। मलिक साहब उधर ही आ रहे थे। सब अदब से खड़े हो गए। सन्नाटा मकड़ी के जाले-सा खिंच गया।
मलिक साहब उनकी अनदेखी करते हुए उस सन्नाटे से गुजर गए। किसी ने धीरे से कहा, ‘काश, हममें से कोई चने वाला होता तो वे हमारी ओर भी देखते।’
मलिक साहब के दिन साहबों की तरह गुजर रहे थे- व्यस्तता और दंबगई से। दस्तखत करते और मीटिंग करते, इसकी सुनते और उसको सुनाते, बिसलरी और नैपकिन का इस्तेमाल करते हुए। एक दिन जब वे दफ्तर से बाहर निकले तो देखा कि पोर्टिको में उनकी कार नहीं थी। सुबह आते समय कार में चम्मच भर खराबी आ गई थी। मलिक साहब ने ड्राइवर से उसे ठीक कराने के लिए कहा था। उसे दफ्तर से अपने लौटने का समय भी दे दिया था। संयोग से आज वे कुछ पहले ही निकल आए थे। ध्यान नहीं था नहीं तो अपने निजी सचिव से पहले पता करवा लेते। अब जब वे बाहर आ गए थे तो दुबारा अपने कमरे में जाने का उनका मन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, कुछ आप-पास का जायजा ही ले लें। इस तरह खुले में निकले बहुत दिन हो गए थे। तभी उनके एक सहयोगी अफसर ने पूछा, ‘मलिक साहब खड़े क्यों हैं ? कार कहीं गई है क्या ? कहाँ चलना है आपको ? आइए, ड्रॉप कर दूँ।’
जवाब में उन्होंने कहा, ‘थैंक्स, आप चलिए। मेरी कार अभी आती होगी।’ मलिक साहब टहलते हुए गेट के बाहर निकले। फुटपाथ पर आए। बाहर गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। लगा, स्टार्ट की सीटी बजते ही वे सब सीना ताने दौड़ पड़ेंगी। वे उधर से होते हुए उसी भवन के दूसरे फाटक के पास पहुँचे। उधर भी काफी गहमागहमी थी। जो भी था, वह बहुत अच्छा था। आस-पास के भवन तो महलों से बढ़कर थे ही, फुटपाथ भी लाजवाब था। उन्हें उस पर चलने का मन हुआ। उनका मन उस वक्त उनके बदन से काफी हलका लग रहा था, हालाँकि उनका बदन भी बुरा नहीं था। काफी तना हुआ तन था। उन्हें आस-पास सब गुब्बारे से लग रहे थे-रंग-बिरंगे, हलके-हलके। एक गुब्बारे वाले को देखकर खयाल आया कि वह कभी भी फट जाता। वैसे आतंकवादी हर किसी को गुब्बारे की तरह ही फोड़ रहे हैं। अचानक उनकी नजर एक चने वाले पर पड़ी। वह अपनी टोकरी सजाए हर आदमी में अपने ग्राहक की संभावना तलाश रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा कुछ था कि मलिक साहब कुछ देर तक उसे देखते रहे। उसे देखकर उन्हें किसी का चेहरा याद आ गया। उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश की। नहीं, यह कोई और था। उन्हें वर्षों पहले के एक दिन की याद आ गई। संयोग से वह घटना इसी जगह घटी थी। वे उस दिन भी इसी फुटपाथ से गुजर रहे थे। वे दिन कुछ और थे। उनकी हैसियत इतनी बड़ी नहीं थी। फुटपाथ की भी हैसियत आज जैसी नहीं थी। दफ्तर से बाहर निकल कर वे किसी वाहन की तलाश कर रहे थे, तभी उन्हें लगा कि कोई उन्हें बुला रहा है वह आवाज ऐसी थी कि उनके बदन में सिरहन दौड़ गई। जैसे अंधेरी रात में किसी बूढ़े पेड़ ने उन्हें पुकारा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उस आदमी को देखकर वे चौंके। उनकी भौंहों पर बल पड़े। वह एक अधेड़ चनेवाला था। उन्हें उसकी गुस्ताखी पर गुस्सा आया। फिर भी वे उसके पास चले गए। उसके बुलावे में कुछ था। पास जाकर पूछा, ‘क्या बात है ?’
चनेवाला क्षण भर उन्हें देखता रहा। वह खुद घबराया-सा था। लगा, कुछ कहते हुए वह हिचक रहा हो। उसने बड़े दबे स्वर में कहा, ‘साहब सुबह से मेरी बोहनी नहीं हुई है। बहुत गरीब आदमी हूँ। मुझसे चने खरीद लीजिए। इसे खाएँगे तो तबियत खुश हो जाएगी। सिर्फ पाँच रूपये !’
मलिक साहब की जिन्दगी में ऐसा प्रस्ताव कभी आया नहीं था। वे अकचका गए। ऐसा कुछ होगा उन्हें उम्मीद नहीं थी। उनके आस-पास काफी साफ सुथरे लोग-आ-जा रहे थे। नजदीक ही गुलदस्ते-सी नजर आनेवाली कुछ लड़कियाँ खड़ी थीं। फिर ऐसी चीजें फुटपाथ पर खरीदने से वे हमेशा बचते थे। ऐसी हालत में इस तरह से किया गया उस चनेवाले का प्रस्ताव उन्हें अनुचित लगा। उन्हें चनेवाले की हिमाकत पर गुस्सा भी आया। चनेवाले ने फिर उसी दयनीयता से कहा, खरीद लो बाबू बहुत गरीब हूँ। माँ कसम, बोहनी नहीं हुई।’
मलिक साहब ने देखा, उसकी लोहे की बालटी भरी हुई थी। एक तरफ नीबू और कुछ कटे प्याज रखे हुए थे, मसाले का एक गंदा-सा डिब्बा भी था। उबले चने मनहूस सूरत लिये पड़े हुए थे। लगा कि वे अपने सार्थक न हो पाने से खुद निराश हो गए हैं। मलिक साहब को याद नहीं पड़ा कि उन्होंने चने कब खाए थे। दरअसल चना उन्हें व्यंजनों में सर्वहारा किस्म का लगता था। वे उन्हें देखकर सहज नहीं हो पाते थे । इसलिए वे चने को करीब देखते तो मना कर देते थे। उस चनेवाले के दयनीय आग्रह का जवाब उन्होंने बहुत रूखाई से दिया। आक्रामक होकर बोले, ‘मैं चने नहीं खाता।’
‘बाबू बहुत गरीब हूँ। कुछ मदद हो जाएगी।’
मलिक साहब खीज गए। वे भुनभुनाते हुए आगे बढ़ गए। मगर चनेवाले की बातें फाँस की तरह उनके मन में गढ़ गईं। वह चेहरा गरमी के आसमान की तरह उनके साथ-साथ चलने लगा। वे कुछ परेशान हो गए गोया कोई फुंसी रगड़ खा-खा हो। एक बार सोचा, लौट जाऊँ, उससे चने न लूँ, पर पाँच रूपए दे दूँ। फिर खयाल आया, वह गरीब है तो क्या, भिखारी तो नहीं। उसका स्वाभिमान भी होगा। उन्हें किसी का सुना हुआ संवाद याद आया, ‘गरीब का अपमान ठीक नहीं।’ फिर सोचा, चने ले लूँ, किसी को दे दूँगा। पर देंगे किसे ? कोई लेगा भी क्यों ? ऐसा कोई उधर नजर भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा, ले लूँ, आगे चलकर फेंक दूँगा। पर यह भी उन्हें नहीं जँचा। फिर उन्होंने सोचा कोई परिचित मिल जाएगा तो उनके हाथ में चने देखकर क्या सोचेगा।
मलिक साहब इसी उधेड़बुन में फँसे रहे। एक अदृश्य जाला उनके चारों ओर फैल गया था। वे फैसला नहीं कर पाए और आगे बढ़ते गए। अचानक उन्हें होश आया। वे काफी दूर चले आए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वह चनेवाला नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने राहत की साँस ली, पर राहत मिली नहीं। हालत यह हुई की घर आकर वे उस चनेवाले की दयनीयता के वायरस से मुक्त नहीं हो पाए। हद तो तब हुई जब सपने में भी उसे यह कहते देखा- ‘बाबू, मैं बहुत गरीब हूँ। सुबह से बोहनी नहीं हुई। पाँच रूपये के चने खा लो।’ वे बड़बड़ाने लगे, ‘मैं चने नहीं खाता।’ मिसेज मलिक कच्ची नींद टूट जाने से नाराज होकर बोलीं, ‘आज रात में तुम्हें चने कौन खिला रहा है ? दिन में तो खाते नहीं। जाने कैसे-कैसे बेहुदे सपने देखते हो। यह लो पानी पीकर करवट लेकर सो जाओ।’ मलिक साहब ने ‘सॉरी कहा, फिर पत्नी के हाथ से पानी लिया और पीकर सो गए।
धीरे-धीरे घटना पुरानी पड़ती गई। समय बीतता रहा उन्हें अपने भीतर एक गंदा कोना नजर आने लगा, जो किसी भी रसायन से साफ नहीं हो रहा था। एक दिन कार से जाते हुए अचानक एक खाली बैठे चनेवाले पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने गाड़ी रूकवाकर उससे चने खरीद लिए और वहीं खड़े एक बच्चे को खिला दिए। धीरे-धीरे यह उनकी आदत बन गई। अब तो जब भी किसी चनेवाले को वे खाली खड़े देखते और वह उन्हें उदास नजर आता तो उससे चने जरूर खरीदते थे। दूसरे क्या सोचेंगे, इसकी चिन्ता उन्हें अब नहीं रह गई थी। उन्हें लगता कि अपना सुकून ही बड़ी बात है और वह भी तब जब वह थोड़े में मिल जाता हो। अभी तक वे अपने खयालों में खोए हुए थे। तभी उन्हें लगा कि कोई उनसे पूछ रहा है, ‘बाबू चने खिलाऊँ ? बढ़िया चने।’ मलिक साहब ने पाया की वे उस चनेवाले के ठीक सामने खड़े थे। उसके मन में कई तरह के विचार आए-गए। फिर कुछ कौतूहल हुआ। उन्होंने अपनी जेब से पाँच का सिक्का निकालकर कहा, ‘आज खिला ही दो, पर देखो इसमें कोई बीमारी न हो। साफ-साफ हों।’ चनेवाला उनकी ओर देखकर मुसकराया। बोला, ‘बाबू साहब, चिंता मत करो। खाओ तब बताना। बीस साल से यहीं पर बाबुओं की सेवा कर रहा हूँ। पहले हमारे बाप भी यहीं पर चने बेचते थे। कभी किसी ने शिकायत नहीं की।’ मलिक साहब ने चुटकी ली, ‘ खानदानी हो।’
चनेवाले ने फुरती से चने में अपना हुनर मिलाया, फिर बड़े संतोष से मलिक साहब को थमा दिया। पहली बार उन्होंने अपने लिए चने लिए थे। ले तो लिए, पर उनकी हिचकिचाहट भी बढ़ गई। खड़े-खड़े सबके सामने खाते हुए उन्हें शर्म आ रही थी। उन्होंने इधर-उधर देखा। पास ही मेंहदी की झाड़ी नजर आई। वे उसकी ओट में चले गए। चारों तरफ उन्होंने एक बार फिर से देखा, जैसे वे किसी व्यस्त चौराहे पर सड़क पार करने की विवशता में हों या किसी निषिद्ध मुहल्ले में गलत काम करने जा रहे हों। उन्होंने झट से उँगलियों से दो चने उठाकर मुँह में डाले। उसका स्वाद लेने की कोशिश की।
तभी अचानक अग्रवाल साहब आते हुए दिखे। वे सीधे उधर ही चले आ रहे थे। वे उनके पुराने साथी थे। बड़े अफसर थे। मलिक साहब ने देखा तो उनके हाथों से चने का ठोंगा छूट गया। मुँह का चना थूककर वे फुरती से आगे बढ़े। सारी चुस्ती के बावजूद उनका शरीर भीतर-ही-भीतर थरथरा रहा था।
अग्रवाल साहब का ध्यान उनकी ओर नहीं था। वे अपने में व्यस्त थे। किसी बड़े साहब की तरह इधर-उधर देखे बिना वे नाक की सीध में आगे बढ़ गए।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book